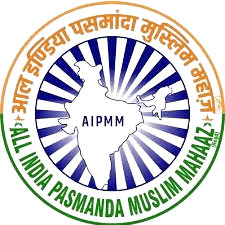भारत का इतिहास केवल सुल्तानों, नवाबों और बादशाहों की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उन मेहनतकश वर्गों की भी कहानी है जिन्होंने अपने परिश्रम, कौशल और रचनात्मकता से इस देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता को स्थायित्व प्रदान किया।
मुस्लिम समाज में यह भूमिका पसमांदा वर्ग ने निभाई — जिनमें अंसारी (जुलाहा), मंसूरी (धुनकर), रंगरेज, दर्जी, कसाई, नाई, तेली, मल्लाह, कुंजड़ा, धोबी, मोची, लुहार और अन्य कारीगर बिरादरियाँ शामिल हैं। इन समुदायों ने बुनाई, चमड़ा-कला, धातु-शिल्प, कृषि और सेवा-क्षेत्रों में अद्भुत योगदान दिया, लेकिन अफ़सोस कि उन्हें सदियों तक सामाजिक-राजनीतिक मुख्यधारा से दूर रखा गया। इतिहास में उनकी भूमिका को दबाया गया, जबकि उनकी मेहनत ने साम्राज्यों को आर्थिक मज़बूती दी।
मुगल काल में सामाजिक विभाजन और पसमांदा की स्थिति
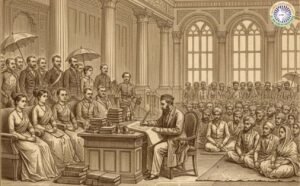 मुगल शासन (1526–1857) में भारतीय मुस्लिम समाज में गहरी जातीय और पेशागत विभाजन रेखाएँ मौजूद थीं। समाज दो प्रमुख वर्गों में बँटा था —
मुगल शासन (1526–1857) में भारतीय मुस्लिम समाज में गहरी जातीय और पेशागत विभाजन रेखाएँ मौजूद थीं। समाज दो प्रमुख वर्गों में बँटा था —
1. अशरफ (श्रेष्ठ वर्ग): ये वे लोग थे जो स्वयं को विदेशी मूल का मानते थे — जैसे सैयद, शेख, पठान, और मुगल। इन्हें शासन, प्रशासन और धार्मिक प्रतिष्ठान के उच्च पद प्राप्त थे। इन्हें “शुद्ध नस्ल” और “पवित्र वंश” के नाम पर श्रेष्ठ समझा जाता था।
2. अजलाफ और अरजाल (पसमांदा वर्ग): ये भारतीय मूल के वे लोग थे जो हिंदू समाज से इस्लाम में धर्मांतरित हुए थे। अजलाफ वर्ग में मध्यम पेशे वाले जैसे जुलाहा, तेली, मल्लाह आदि आते थे, जबकि अरजाल वर्ग में धोबी, कसाई, मोची और नाई जैसे पेशागत रूप से नीची मानी जाने वाली बिरादरियाँ थीं। इन समुदायों को “अशरफ” वर्ग से विवाह या सामाजिक मेलजोल की अनुमति नहीं थी। मुगल शासन में अशरफ वर्ग प्रशासनिक और सैन्य पदों पर काबिज़ था, जबकि पसमांदा वर्ग बुनाई, कृषि, पशुपालन, कारीगरी और श्रम जैसे कार्यों तक सीमित था। मुगल शहरों—दिल्ली, आगरा, लाहौर, और फैज़ाबाद—में अशरफों की हवेलियाँ थीं, वहीं पसमांदा समाज के लोग शहरों के बाहरी हिस्सों या झुग्गियों में रहते थे। उनके कौशल—जैसे बनारसी साड़ी की बुनाई, धातु-कला और रंगाई—ने मुगल अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाया, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं मिला। उनके लिए उच्च शिक्षा या प्रशासनिक सेवा तक पहुँच लगभग असंभव थी।
ब्रिटिश काल में पसमांदा समाज की आर्थिक और सामाजिक उन्नति : जब मुगल सत्ता ढही और ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, तब मुस्लिम समाज में नई सामाजिक गतिकी उत्पन्न हुई। अशरफ वर्ग, जो सत्ता के साथ सदैव जुड़ा था, ने अंग्रेजों की दलाली शुरू कर दी और सिविल सेवा, सेना तथा प्रशासनिक पदों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरी ओर, पसमांदा समाज ने अपने श्रम और कौशल पर भरोसा किया। बनारस, भागलपुर, पटना, मुरादाबाद, आज़मगढ़, मऊ, और फिरोज़ाबाद जैसे शहरों में अंसारी, मंसूरी, मोची, लुहार और रंगरेज बिरादरियों ने हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और धातु-कला में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि ब्रिटिश नीतियाँ—जैसे मैनचेस्टर के कपड़ों का आयात—भारतीय बुनकरों के लिए विनाशकारी साबित हुईं, फिर भी इन समुदायों ने संघर्ष करके जीविका का मार्ग निकाला। इस काल में पसमांदा समाज की जीवटता देखी जा सकती है — उन्होंने अपने पारंपरिक पेशों को संरक्षित रखते हुए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग खोजा।
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पसमांदा समाज की भूमिका
1857 का संग्राम केवल सैनिक बगावत नहीं था; यह जन-आंदोलन था जिसमें पसमांदा समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस जैसे केंद्रों में जुलाहा (अंसारी), धुनकर, कसाई और धोबी समुदायों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
इन लोगों ने न केवल हथियार उठाए, बल्कि आर्थिक सहायता, रसद, भोजन और वस्त्रों का भी प्रबंध किया। लेकिन जब ब्रिटिश शासन ने क्रांति को कुचल दिया, तो बदले में इन्हीं मेहनतकशों पर अत्याचार किया गया।
सर सैयद अहमद खान और वर्गीय विभाजन की स्थायी नींव : विद्रोह के बाद सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक “असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद” (1859) में लिखा कि यह बगावत “जुलाहों और निम्न वर्ग के मुसलमानों” द्वारा की गई थी।
उन्होंने अशरफों को निर्दोष बताया और ब्रिटिशों को विश्वास दिलाया कि “असली मुसलमान” यानी अशरफ उनके विरोधी नहीं हैं। इस रुख का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने पसमांदा मुसलमानों को सज़ा दी — उनके करघे तोड़े गए, उद्योगों को बंद कराया गया, और आर्थिक रूप से उन्हें अपंग बना दिया गया। जबकि अशरफ वर्ग को अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से पुनः सत्ता और शिक्षा के द्वार खोल दिए गए।
अलीगढ़ आंदोलन और शिक्षा में असमानता : सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मदरसा-उल-उलूम (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) ने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। लेकिन यह शिक्षा मुख्यतः अशरफ मुस्लिमों तक सीमित रही। पसमांदा समाज, जो या तो कारीगर या मज़दूर वर्ग था, आर्थिक कारणों से इन संस्थानों तक नहीं पहुँच सका। इससे मुस्लिम समाज में शैक्षणिक विषमता गहरी होती गई। आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में पसमांदा मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत अत्यंत कम है, जबकि अशरफ वर्ग नेतृत्व और शिक्षण पदों पर अधिक संख्या में मौजूद है।
💼 आर्थिक स्थिति और रोज़गार : पसमांदा समाज का आर्थिक ढाँचा श्रम आधारित रहा है। इनकी प्रमुख जीविकाएँ — बुनाई, दर्जीगिरी, कसाईगिरी, नाव-चालन, कृषि और चमड़ा-उद्योग — औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश आयात नीति के कारण धीरे-धीरे प्रभावित हुईं। इन पेशों में मजदूरी अस्थिर और आय सीमित रही, जिससे गरीबी और ऋणग्रस्तता ने घर कर लिया। आज भी यह वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ न तो श्रम-सुरक्षा है, न न्यूनतम वेतन।
राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय : मुगल और ब्रिटिश काल दोनों में पसमांदा समाज राजनीतिक शक्ति से वंचित रहा। अशरफ मुस्लिमों ने अपने प्रभाव और शिक्षा के बल पर नेतृत्व पर एकाधिकार बना लिया। आज़ादी के बाद भी यही स्थिति जारी रही — मुस्लिम राजनीति में नेतृत्व मुख्यतः सैयद, शेख और पठान बिरादरियों के हाथ में रहा, जबकि पसमांदा समाज मतदाता और भीड़ के रूप में इस्तेमाल होता रहा। “पसमांदा आंदोलन” ने इस असमानता को उजागर किया और यह कहा कि मुस्लिम समाज एकसमान नहीं, बल्कि जातीय रूप से विभाजित है। इस आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय में समान अवसर प्राप्त करना है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temperament) : पसमांदा समाज की बड़ी आबादी ग्रामीण या झुग्गी-बस्ती क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं। मातृ-मृत्यु दर, कुपोषण, और स्वास्थ्य-सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ व्यापक हैं। शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temperament) विकसित नहीं हो पाया। पसमांदा महाज़ जैसी संस्थाएँ अब समाज में तर्क-आधारित सोच, आधुनिक शिक्षा और स्वावलंबन का संदेश प्रसारित कर रही हैं, ताकि धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
🌾 पसमांदा समाज का वर्तमान योगदान और दिशा : आज पसमांदा मुसलमान देश की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% हैं। ये कृषि, उद्योग, सेवा, और लघु व्यवसाय क्षेत्रों में रीढ़ की हड्डी के समान भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी वे शिक्षा, रोजगार, और प्रतिनिधित्व में पिछड़े हुए हैं। इसीलिए ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ जैसे संगठन सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक चेतना, आर्थिक सशक्तिकरण, और तालीमी बिदारी पर निरंतर काम कर रहे हैं। मुगल काल की सामाजिक असमानता से लेकर ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक शोषण नीति और स्वतंत्र भारत की राजनीतिक उपेक्षा तक पसमांदा मुस्लिम समाज ने हर दौर में संघर्ष किया, योगदान दिया और अपनी मेहनत से देश की प्रगति में भागीदारी निभाई।
अब समय आ गया है कि इतिहास को नए दृष्टिकोण से लिखा जाए — जिसमें राजाओं के साथ उन मेहनतकश हाथों की भी दास्तान दर्ज हो, जिन्होंने सभ्यता को जीवन दिया। पसमांदा समाज भारत की आत्मा है — उनका सम्मान, समानता और अवसर ही सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का आधार बन सकता है।

मुहम्मद यूनुस
मुख्य कार्यकारी निदेशक,
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़