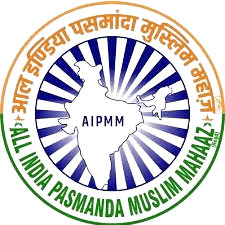भारत की आज़ादी को 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति एक “चेहरों की राजनीति” में उलझी हुई है। हर दौर में मुसलमानों के सामने एक “अपना चेहरा” रखा गया, लेकिन अपना नेतृत्व कभी नहीं दिया गया।राजनीति में हिस्सेदारी तो दिखाई दी, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति कभी उनके हाथों में नहीं आई।
एक ऐतिहासिक मिसाल- साल 1998 का लोकसभा चुनाव — उत्तर प्रदेश का रामपुर संसदीय क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यहां से मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बनाया। वे इलाहाबाद के रहने वाले थे, रामपुर के नहीं — यानी एक “पैराशूट उम्मीदवार”। उनका मुकाबला था बेगम नूर बानो से, जो नवाबी वंश से ताल्लुक रखती थीं और पहले से सांसद थीं। भाजपा ने मुसलमानों के बीच “मुस्लिम चेहरा” दिखाकर प्रचार किया — और परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने मुस्लिम-बहुल सीट पर अप्रत्याशित जीत हासिल की। उस दौर के एक भाजपा नेता का यह कथन आज भी सटीक प्रतीत होता है:
> “हिंदू नेतृत्व देखता है, मुसलमान चेहरा।” यही वाक्य मुसलमानों की पूरी राजनीतिक यात्रा का सार है — हम चेहरों के पीछे भागते रहे, नेतृत्व कभी नहीं मांगा।
चेहरों की राजनीति का भ्रम
 स्वतंत्रता के बाद से आज तक तथाकथित सेक्युलर पार्टियों — कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी — सभी ने मुसलमानों को केवल चेहरे के रूप में इस्तेमाल किया, नेतृत्व कभी नहीं दिया।
स्वतंत्रता के बाद से आज तक तथाकथित सेक्युलर पार्टियों — कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी — सभी ने मुसलमानों को केवल चेहरे के रूप में इस्तेमाल किया, नेतृत्व कभी नहीं दिया।
उन पार्टियों में मुस्लिम मंत्री, सांसद और विधायक तो बने, लेकिन नीति और निर्णय की बागडोर हमेशा उस पार्टी के नेतृत्व के हाथ में रही।
इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो दिखा, पर सत्ता में वास्तविक साझेदारी नहीं मिल सकी।
नेतृत्व बनाम चेहरा- चेहरा केवल जनता को प्रभावित करने का माध्यम होता है, जबकि नेतृत्व वह शक्ति है जो नीतियां और दिशा तय करता है।
चेहरा मंच पर ताली पाता है,
नेतृत्व नीति में हस्ताक्षर करता है।
जब तक चेहरा उपयोगी है, सम्मानित है;
जब पार्टी को लगे कि उसकी “वोट वैल्यू” घट गई है,
वही चेहरा “बोझ” बन जाता है।
कुछ उदाहरण जो बहुत कुछ कहते हैं- बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी “मुस्लिम चेहरा” माने जाते थे, इसी प्रकार से बीजेपी के सैय्यद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी भी मुस्लिम चेहरा माने जाते थे,लेकिन जब नेतृत्व ने महसूस किया कि अब उनका लाभ नहीं रहा, उन्हें बाहर कर दिया गया या साइड में बिठा दिया गया। सपा में आज़म खान, राजद में मोहम्मद शहाबुद्दीन, और एनसीपी में तारिक अनवर — सभी प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे रहे, लेकिन पार्टी की नीति-निर्माण प्रक्रिया से हमेशा बाहर रखे गए। सपा के संस्थापक सदस्य होने के बावजूद आज़म खान कभी निर्णायक नेतृत्व नहीं बन पाए — क्योंकि नेतृत्व हमेशा यादव परिवार के हाथों में सिमटा रहा।
नेतृत्व की ताकत बनाम चेहरों की बेबसी
राजनीति में चेहरा केवल “मोहरा” होता है, जबकि नेतृत्व सियासत की असली बिसात का खिलाड़ी।
पत्रकार राजीव रंजन ने अपने पॉडकास्ट में बताया: “जब सपा में आज़म खान और अमर सिंह के बीच मतभेद हुआ, तो मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया कि सभी मुस्लिम नेता अमर सिंह का साथ दें। किसी ने आज़म खान का समर्थन नहीं किया।
बाद में जब पार्टी को लगा कि अब आज़म की वापसी फ़ायदेमंद है, तो वही नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर सिंह के खिलाफ बोलते दिखे।” यह उदाहरण दिखाता है कि चेहरा केवल आदेश का पालन करता है, वह निर्णय नहीं लेता, केवल निर्णय झेलता है।
मुस्लिम राजनीति की विफलता की जड़- आज़ादी के बाद से अब तक सैकड़ों मुस्लिम सांसद और विधायक संसद व विधानसभाओं में पहुंचे, लेकिन क्या मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोज़गार या सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ? नहीं। क्योंकि वे “पार्टी लाइन” के बंधन में रहे, अपने समाज के सवालों पर कभी एकजुट नहीं हुए। इसके विपरीत, दलित और पिछड़े वर्गों के नेता अपने समुदाय के अधिकारों के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी संघर्ष करते रहे —
क्योंकि उनके पास नेतृत्व की चेतना थी, केवल “चेहरा” नहीं।
आज की राजनीतिक वास्तविकता आज भी देश के देश के कई राज्यों में मुसलमानों मारपीट गलीगलौज के साथ साथ उनको को लेकर अपमानजनक बयान दिए जाते हैं, लेकिन तथाकथित “सेक्युलर” दलों के मुस्लिम चेहरे या तो चुप रहते हैं या पार्टी की भाषा दोहराते हैं। उनकी निष्ठा “पार्टी” के प्रति होती है, समाज के प्रति नहीं।
सच्चाई यह भी है… जो भी नेता मुसलमानों के असली मुद्दों पर बोलता है — जैसे असदुद्दीन ओवैसी, या पहले मुस्लिम लीग के नेता — उसे तुरंत “भाजपा का एजेंट”, “वोटकटवा” या “कट्टरपंथी” कह दिया जाता है। जबकि वही नेता कम से कम मुस्लिम मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में लाते हैं। बाकी “चेहरे” केवल ताली बजाने तक सीमित रहते हैं। अब वक्त है नेतृत्व गढ़ने का मुस्लिम समाज को अब चेहरों की राजनीति से निकलकर नेतृत्व निर्माण की दिशा में बढ़ना होगा।
नेतृत्व का अर्थ है — अपने राजनीतिक एजेंडे को तय करने की ताकत, नीति निर्धारण में भागीदारी की क्षमता, और सरकार से संवाद (Negotiation) करने का साहस। बिना नेतृत्व के हम हमेशा “मांगने वाले” रहेंगे — सत्ता में साझेदार नहीं बन पाएंगे
महाज़ की भूमिका: नेतृत्व निर्माण की ओर एक संगठित प्रयास ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ इसी दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है। महाज़ का मानना है कि पसमांदा समाज को अब सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि नेतृत्व चाहिए।
महाज़ देश के 12 राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से पसमांदा समाज को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में जुटा है।
संगठन का उद्देश्य है — मुसलमानों में आत्मनिर्भर नेतृत्व तैयार करना, जो न केवल अपने समाज की आवाज़ बने, बल्कि नीति-निर्माण में साझेदारी और मोलभाव (Bargaining Power) की ताकत रखे।
भविष्य की दिशा: सत्ता में साझेदारी, न कि सत्ता की मांग महाज़ का मानना है कि संगठन का लक्ष्य सरकार बनाना नहीं, बल्कि आने वाली कोलिशन सरकारों में निर्णायक भूमिका निभाना है। भारत का राजनीतिक भविष्य सहयोगी सरकारों (Coalition Governments) का है। ऐसे में पसमांदा समाज यदि संगठित नेतृत्व के साथ आगे बढ़े, तो वह किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर सार्थक संवाद और सौदेबाज़ी (Negotiation) कर सकता है।
यही सच्चा नेतृत्व है — जो “वोट बैंक” नहीं, नीति-निर्माण का भागीदार बन सके। > “अगर सियासी ताकत चाहिए, तो चेहरों के मोह से निकलकर नेतृत्व गढ़िए।” चेहरे आते-जाते रहेंगे, लेकिन नेतृत्व ही स्थायी शक्ति बनेगा।
अब समय है कि मुस्लिम समाज दूसरों की पार्टियों में “चेहरा” बनने के बजाय अपना राजनीतिक ढांचा, अपना एजेंडा, और अपना नेतृत्व खड़ा करे।
तभी बदलाव आएगा — वरना “चेहरे” बदलते रहेंगे, और “हालात” वही के वही रहेंगे
 मुहम्मद यूनुस
मुहम्मद यूनुस
चीफ़ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़