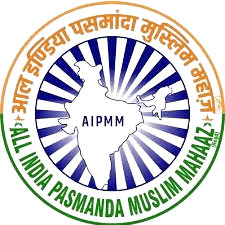समकालीन भारतीय सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में, मुस्लिम समुदाय स्वयं को पहचान, हाशिए पर होने, आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक कलह और बहुलवाद के लिए खतरों के एक जटिल जाल में फँसा हुआ पाता है। चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, जिनमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अधिकारों से वंचित होना और शैक्षिक पिछड़ापन से लेकर मीडिया द्वारा गलत प्रस्तुति और वैचारिक दुरुपयोग तक शामिल हैं। फिर भी, इन कठिनाइयों के बीच, कुरान एक स्पष्ट नैतिक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसे यदि ईमानदारी से अपनाया जाए, तो यह मुसलमानों को समृद्धि की ओर ले जाने वाले एक दिशासूचक के रूप में कार्य कर सकता है और साथ ही राष्ट्रीय विकास में भी योगदान दे सकता है। दया (रहमा), न्याय (अदल) और करुणा (एहसान) के मूलभूत विषय इस्लाम में गौण गुण नहीं हैं; ये इसका सार हैं। ये मूल्य न केवल ईश्वरीय गुण हैं, बल्कि विश्वासियों के लिए नैतिक अनिवार्यताएँ भी हैं, जो व्यक्तिगत आचरण और सामूहिक कार्य दोनों का मार्गदर्शन करती हैं।
पवित्र कुरान बार-बार पुष्टि करता है कि दया सृष्टि के साथ ईश्वरीय जुड़ाव का सर्वव्यापी सिद्धांत है। सूरह अल-अराफ़ (7:156) में अल्लाह ने घोषणा की है, “मेरी दया हर चीज़ को घेरे हुए है।” यह आयत किसी धार्मिक अमूर्तता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह घोषणा करती है कि दया मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), जिन्हें “सारे संसारों के लिए दया” (21:107) कहा गया है, ने मित्रों और शत्रुओं, दोनों के साथ अपने व्यवहार में इस सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत किया। मक्का की विजय के दौरान कुरैश को क्षमा करना, अनाथों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति उनकी करुणा, और मदीना में उनका समावेशी शासन नैतिक नेतृत्व के चिरस्थायी आदर्श हैं। ये उदाहरण न केवल ऐतिहासिक अनुस्मारक के रूप में, बल्कि आधुनिक समय में मुसलमानों के आचरण के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश भी हैं। बहुलवादी भारत में रहने वाले मुसलमानों को इन आयतों की प्रासंगिकता को समझना चाहिए। मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे जीवन जिएँ और सेवा करें मानो वे कुरान और पैगंबर की सुन्नत के जीवित अवतार हों। न्याय कुरान का दूसरा जीवित अवतार और प्रतिमान है। यह केवल कानूनी न्यायनिर्णयन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र सिद्धांत है जिसमें सामाजिक समता, निष्पक्षता और नैतिक अखंडता समाहित है। ईश्वर 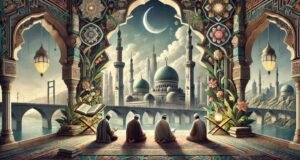 ईमान वालों से कहता है कि “अमानत को उन लोगों को लौटा दो जिनके वे हक़दार हैं; और जब तुम लोगों के बीच न्याय करो, तो न्याय से न्याय करो” (4:58)। एक अन्य आयत में कहा गया है कि न्याय को कायम रखना चाहिए, भले ही वह स्वयं के या अपने परिवार के विरुद्ध हो। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे अमीर और गरीब, दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह निर्देश ऐसे संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहाँ मुसलमानों को व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को न्याय में बाधा नहीं बनने देना चाहिए, भले ही वे स्वयं को पीड़ित पाते हों। पूर्वाग्रह, सामाजिक बहिष्कार और हानि का भय उन्हें सार्वजनिक भलाई करने से नहीं रोकना चाहिए, भले ही वह उन्हें वंचित कर दे। कुरान आगे निर्देश देता है, “किसी जाति के प्रति घृणा तुम्हें न्याय करने से न रोके; न्याय करो: यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है” (5:8)। यह आयत प्रतिशोधात्मक अन्याय के किसी भी औचित्य को समाप्त करती है और इस बात की पुष्टि करती है कि शत्रुता के बावजूद भी न्याय को कायम रखा जाना चाहिए। भारतीय मुसलमानों के लिए, इस तरह के व्यवहार का अर्थ है न्यायिक व्यवस्था से जुड़ना, कानूनी संस्थाओं द्वारा दिए गए फैसलों का पालन करना, संवैधानिक अधिकारों की वकालत करना और उकसावे का प्रतिक्रियावादी उत्साह से जवाब देने के प्रलोभन का विरोध करना।
ईमान वालों से कहता है कि “अमानत को उन लोगों को लौटा दो जिनके वे हक़दार हैं; और जब तुम लोगों के बीच न्याय करो, तो न्याय से न्याय करो” (4:58)। एक अन्य आयत में कहा गया है कि न्याय को कायम रखना चाहिए, भले ही वह स्वयं के या अपने परिवार के विरुद्ध हो। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे अमीर और गरीब, दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह निर्देश ऐसे संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहाँ मुसलमानों को व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को न्याय में बाधा नहीं बनने देना चाहिए, भले ही वे स्वयं को पीड़ित पाते हों। पूर्वाग्रह, सामाजिक बहिष्कार और हानि का भय उन्हें सार्वजनिक भलाई करने से नहीं रोकना चाहिए, भले ही वह उन्हें वंचित कर दे। कुरान आगे निर्देश देता है, “किसी जाति के प्रति घृणा तुम्हें न्याय करने से न रोके; न्याय करो: यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है” (5:8)। यह आयत प्रतिशोधात्मक अन्याय के किसी भी औचित्य को समाप्त करती है और इस बात की पुष्टि करती है कि शत्रुता के बावजूद भी न्याय को कायम रखा जाना चाहिए। भारतीय मुसलमानों के लिए, इस तरह के व्यवहार का अर्थ है न्यायिक व्यवस्था से जुड़ना, कानूनी संस्थाओं द्वारा दिए गए फैसलों का पालन करना, संवैधानिक अधिकारों की वकालत करना और उकसावे का प्रतिक्रियावादी उत्साह से जवाब देने के प्रलोभन का विरोध करना।
करुणा कुरान में व्यक्त तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो दया और न्याय के बीच भावनात्मक और नैतिक सेतु है। करुणा में दया को क्रियान्वित करते हुए न्याय को मानवीय बनाने का एक सहज गुण है। कुरान कहता है, “जो लोग धरती पर विनम्रता से चलते हैं और जब अज्ञानी उन्हें संबोधित करते हैं, तो वे शांति के शब्दों के साथ जवाब देते हैं” (25:63)। यह आयत जटिल सामाजिक परिदृश्य में मार्गदर्शन के लिए एक नैतिक दिशासूचक प्रदान करती है। इस आयत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक विमर्श में उकसावे और पूर्वाग्रहों का आक्रामक तरीके से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। संयम बरतना चाहिए, और अज्ञानता और शत्रुता का सामना करते समय भी गरिमा और शांति के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान किया जाना चाहिए। करुणा को कमज़ोरी के बराबर नहीं माना जा सकता, बल्कि यह शक्ति, सहानुभूति और मध्यमार्ग है, जो मनुष्य को गलत और सही में अंतर करने में सक्षम बनाता है। यह वह शक्ति है जो विरोधियों को मित्र में और संघर्ष को सह-अस्तित्व में बदल देती है।
आज भारतीय मुसलमान केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो अधिक चिंताजनक हैं। शैक्षिक मानकों का क्षरण, नैतिक मूल्यों का ह्रास और सांप्रदायिक एकता का विखंडन गंभीर चिंता का विषय हैं। कुरान इन मुद्दों को निंदा के माध्यम से नहीं, बल्कि रचनात्मक मार्गदर्शन के माध्यम से संबोधित करता है। कुरान पूछता है, “क्या जो जानते हैं वे उन लोगों के बराबर हैं जो नहीं जानते?” यह प्रश्न ज्ञान के मूल्य और बौद्धिक जुड़ाव की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। इसलिए शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। भारतीय मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शिक्षा, दोनों में निवेश करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके युवा एक प्रतिस्पर्धी और नैतिक रूप से जटिल दुनिया में फलने-फूलने के लिए आवश्यक कौशल और नैतिकता।
क़ुरान इन तीन गुणों को एकता के व्यापक दायरे में समाहित करता है, जिसे समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली अनिवार्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। क़ुरान मुसलमानों को अराजकता और विभाजन न फैलाने का आदेश देता है, क्योंकि जो लोग जानबूझकर विभाजन पैदा करते हैं, वे उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं जिसने मानवता को एक बनाया है। सांप्रदायिकता, वैचारिक कठोरता और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता ने सामूहिक शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। क़ुरान एकरूपता का नहीं, बल्कि विविधता में एकता का आह्वान करता है, जो साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित हो। इस एकता को न केवल धार्मिक स्थलों में, बल्कि नागरिक जुड़ाव, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सक्रियता में भी विकसित किया जाना चाहिए। एक एकजुट समुदाय अपने अधिकारों की वकालत करने, राष्ट्रीय विकास में योगदान देने और विभाजनकारी आख्यानों का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में होता है।
क़ुरान प्रतिक्रिया के बजाय सुधार की रणनीति की वकालत करता है “बुराई को बेहतर चीज़ से दूर करो; फिर जो तुम्हारा दुश्मन था वह तुम्हारे घनिष्ठ मित्र जैसा करीबी बन जाएगा।” यह आयत नैतिक आचरण की परिवर्तनकारी शक्ति को अभिव्यक्त करती है और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सहभागिता, संवाद और नैतिक उत्कृष्टता का आह्वान करती है। भारतीय मुसलमानों को पीड़ित होने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और इसके बजाय रचनात्मक कार्यों, जैसे कानूनी वकालत, मीडिया साक्षरता, अंतर्धार्मिक संवाद और नागरिक भागीदारी, के माध्यम से अपनी क्षमता का दावा करना चाहिए। इसका लक्ष्य केवल अधिकारों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ न्याय, दया और करुणा आदर्श हों।
मुहम्मद सलीम,
पीएचडी एवं शोध सहयोगी, आईसीएसएसआर