भारत दुनिया में बहुलवादी समाज के सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक है, एक ऐसा देश जहाँ एकता विविधता को मिटा नहीं पाती और विविधता एकता को विभाजित नहीं करती। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर तमिलनाडु के तटीय मंदिरों तक, दिल्ली के सूफी दरगाहों से लेकर लद्दाख के मठों तक, भारतीय परिदृश्य सह-अस्तित्व की एक शाश्वत कहानी कहता है। भारत की संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित बहुलवाद की यह भावना इसकी राष्ट्रीय पहचान और नैतिक शक्ति को परिभाषित करती रही है।
भारत में बहुलवाद कोई नया राजनीतिक विचार नहीं है; यह हज़ारों वर्षों से पोषित एक सभ्यतागत लोकाचार है। प्राचीन भारतीय कहावत, “एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति”, सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान लोग इसे कई तरीकों से वर्णित करते हैं, इस दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करती है। सदियों से, भारत ने दूर-दराज के देशों से आए व्यापारियों, यात्रियों, शरणार्थियों और विचारकों का स्वागत किया है, जिन्हें अपने धर्मों और रीति-रिवाजों के लिए स्वीकृति और सम्मान मिला। एकरूपता थोपने की कोशिश करने वाले समाजों के विपरीत, भारत ने विविधता को ज्ञान के स्रोत के रूप में मनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और अन्य धर्म सह-अस्तित्व में रहे हैं और अक्सर एक-दूसरे की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में योगदान करते रहे हैं। भारत की समन्वित भाषाएँ, त्यौहार, संगीत और व्यंजन इस साझा विरासत को दर्शाते हैं।
 किसी भी भारतीय शहर में घूमिए, आपको इस साझा विरासत के चिन्ह हर जगह दिखाई देंगे। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वालियाँ सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करती हैं; हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण किया, जो पहचान से परे एक उत्कृष्ट कृति है; और केरल में, हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का सदियों पुराना सह-अस्तित्व अद्वितीय कला रूपों और साझा रीति-रिवाजों को जन्म देता रहा है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर, वाराणसी में, मंदिर की घंटियाँ मुअज़्ज़िन की पुकार के साथ सहज रूप से घुल-मिल जाती हैं। पंजाब में, सिख लंगर बिना किसी भेदभाव के सभी पृष्ठभूमि के लोगों को भोजन कराते हैं। पूरे पूर्वोत्तर में, आदिवासी परंपराएँ आधुनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारत की विविधता एक बोझ नहीं, बल्कि परस्पर निर्भरता और सम्मान का जीवंत संगम है।
किसी भी भारतीय शहर में घूमिए, आपको इस साझा विरासत के चिन्ह हर जगह दिखाई देंगे। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वालियाँ सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करती हैं; हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण किया, जो पहचान से परे एक उत्कृष्ट कृति है; और केरल में, हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का सदियों पुराना सह-अस्तित्व अद्वितीय कला रूपों और साझा रीति-रिवाजों को जन्म देता रहा है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर, वाराणसी में, मंदिर की घंटियाँ मुअज़्ज़िन की पुकार के साथ सहज रूप से घुल-मिल जाती हैं। पंजाब में, सिख लंगर बिना किसी भेदभाव के सभी पृष्ठभूमि के लोगों को भोजन कराते हैं। पूरे पूर्वोत्तर में, आदिवासी परंपराएँ आधुनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारत की विविधता एक बोझ नहीं, बल्कि परस्पर निर्भरता और सम्मान का जीवंत संगम है।
भारत का इतिहास परस्पर संवाद और पारस्परिक समृद्धि की कहानियों से भरा पड़ा है। भारतीय वास्तुकला पर फ़ारसी प्रभाव, संस्कृत और फ़ारसी का सम्मिश्रण जिसने उर्दू को जन्म दिया, और मुस्लिम उस्तादों और हिंदू संगीतकारों के योगदान से शास्त्रीय संगीत का विकास, ये सभी दर्शाते हैं कि भारत में संस्कृतियों में कभी टकराव नहीं हुआ, बल्कि संवाद हुआ। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इस सद्भाव को और गहरा किया। कबीर, गुरु नानक और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने प्रेम की ऐसी भाषा बोली जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से परे थी। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि भक्ति और मानवता, कर्मकांड या पहचान से कहीं बढ़कर हैं। यह साझा आध्यात्मिक विरासत भारत की सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है।
भारत का कैलेंडर विविधता का एक वर्ष भर चलने वाला उत्सव है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ओणम, होली और पोंगल, धर्म की परवाह किए बिना, आपसी भागीदारी के साथ मनाए जाते हैं। कई गाँवों में, हिंदू परिवार ईद पर सेवइयाँ बनाते हैं, जबकि मुस्लिम पड़ोसी दिवाली पर दीये जलाते हैं। ये छोटे-छोटे मगर गहरे भाव, उस विश्वास और स्नेह का प्रतीक हैं जो भारतीय समाज की रीढ़ हैं। भारत में त्यौहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि सामूहिक आनंद और मानवता की अभिव्यक्ति हैं। ये सह-अस्तित्व, उदारता और दूसरों के साथ खुशियाँ बाँटने का महत्व सिखाते हैं।
भारत का बहुलवाद अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों में फलता-फूलता है। इसका संगीत, साहित्य और व्यंजन सदियों पुराने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाते हैं। सितार, तबला और ग़ज़ल में विभिन्न परंपराओं के अंश एक ही धुन में समाहित हैं। साहित्य में, मीर और ग़ालिब जैसे उर्दू कवि, कालिदास जैसे संस्कृत विद्वान, और तमिल, बंगाली या मलयालम के आधुनिक लेखकों ने भारत की सामूहिक पहचान में अनूठी आवाज़ें जोड़ी हैं। यहाँ तक कि व्यंजनों में भी, क्षेत्रीय और धार्मिक प्रभाव खूबसूरती से घुल-मिल गए हैं। मुगलई बिरयानी, गोवा की फिश करी, कश्मीरी कहवा और गुजराती ढोकला अलगाव के नहीं, बल्कि साझा विकास के प्रतीक हैं। प्रत्येक व्यंजन समुदायों के बीच प्रवास, अनुकूलन और स्नेह की कहानी कहता है।
1950 में अपनाए गए भारत के संविधान ने उस बहुलवादी भावना को औपचारिक अभिव्यक्ति दी जिसने लंबे समय से इस उपमहाद्वीप को परिभाषित किया था। यह धर्म, अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ये ऐसे मूल्य हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत विविधता फलती-फूलती रहे। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि भारत की ताकत समावेशिता में है, न कि एकरूपता में। इसलिए, बहुलवाद केवल एक सांस्कृतिक घटना ही नहीं, बल्कि एक नैतिक और कानूनी प्रतिबद्धता भी है। यह यह सुनिश्चित करके भारत के लोकतंत्र को बनाए रखता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, समान अधिकार और सम्मान प्राप्त करे। हाल के दिनों में, सामाजिक ध्रुवीकरण और गलत सूचनाओं ने कभी-कभी इस सद्भाव की परीक्षा ली है। हालाँकि, अधिकांश भारतीय सह-अस्तित्व के सिद्धांतों को कायम रखते हैं। अब यह ज़िम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है कि वह विभाजनकारी आख्यानों को अस्वीकार करे, संवाद के सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करे और युवा पीढ़ी को सहिष्णुता और सहानुभूति के मूल्यों से परिचित कराए। बहुलवाद को केवल कानूनों से ही संरक्षित नहीं किया जा सकता; यह लोगों के दैनिक कार्यों, पड़ोसियों के प्रति दया, विभिन्न विश्वासों के प्रति सम्मान और आलोचना करने के बजाय सुनने की इच्छा से पनपता है।
भारत का बहुलवाद केवल कंधे से कंधा मिलाकर रहने के बारे में नहीं है; यह आपसी सम्मान और साझा उद्देश्य के साथ साथ रहने के बारे में है। यह जीवन जीने का एक तरीका है।
जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे विरोध में नहीं, बल्कि सद्भाव में खड़े हों। भारतीय भावना सिखाती है कि एकता एकरूपता नहीं, बल्कि स्वीकृति है, कि आस्थाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल एक हो सकते हैं। पहचान से लगातार विभाजित होती दुनिया में, भारत एक प्राचीन लेकिन शाश्वत सबक देता है: शक्ति विविधता में, शांति समझ में और महानता एकजुटता में निहित है। इस बहुलवादी विरासत को संरक्षित रखना भारत का कर्तव्य ही नहीं, बल्कि विश्व को भारत का उपहार है।

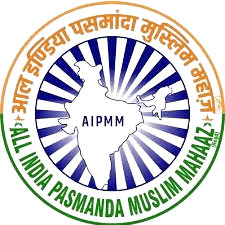
परम्परा मुजब भारत देश में सभी धर्म का सम्मान किया जाता था वक्त के साथ हालात बदलते गए आज भी कुछ लोगों के द्वारा सभी धर्म का सम्मान किया जा रहा है भारत देश में सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए यही देश में शांति एकता भाईचारा का संदेश है आपस में कुछ मसलों पर भेद भाव तो हो सकते हैं लेकिन हिन्द कि धरती पर कही धर्म के लोग अपना धर्म निभा रहा है।। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ओबीसी सलीम गरासिया प्रदेश अध्यक्ष गुजरात 🙏