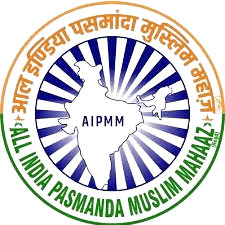भारत के विविध मुस्लिम समाज के हृदय में एक असहज सच्चाई छिपी हुई है — एक गहराई तक जमी हुई जातिगत संरचना, जो न केवल इस्लाम की समानता की भावना का उल्लंघन करती है, बल्कि भारतीय संविधान के न्याय और समानता के वादे का भी।
यह लेख परिवर्तन की एक पुकार है — पासमांदा मुसलमानों की पहचान और सशक्तिकरण की अपील, जो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह इतिहास, संविधान और नैतिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज में एक नए सामाजिक जागरण और नेतृत्व परिवर्तन का आह्वान करता है।
धर्म से विश्वासघात: मुसलमानों में जाति की जड़ें
पवित्र कुरआन की सूरह अल-हुजुरात (49:13) में एक शाश्वत सत्य प्रकट किया गया है —
“हे मनुष्यों! निस्संदेह हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें जातियों और कबीलों में बाँटा ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान सको। निश्चय ही अल्लाह के निकट सबसे सम्मानित वह है जो सबसे अधिक धर्मनिष्ठ है।”
यह दिव्य संदेश जन्म, वंश या सामाजिक स्थिति पर आधारित हर प्रकार की ऊँच-नीच को अस्वीकार करता है। लेकिन भारत में, एक जाति जैसी व्यवस्था मुसलमानों के बीच अब भी बनी हुई है — जो इस्लाम की शिक्षाओं और भारतीय धर्मनिरपेक्षता दोनों के विपरीत है।
 इतिहास में यह विभाजन उस समय शुरू हुआ जब 8वीं सदी में इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में आया। अरब, फारसी और मध्य एशियाई अभिजात वर्ग — जो अक्सर खुद को अशराफ (उच्च कुलीन) कहते थे — स्थानीय लोगों से मिले, जिनमें अधिकतर वे निम्नवर्गीय हिंदू थे जो ब्राह्मणवादी उत्पीड़न से मुक्ति चाहते थे। समय के साथ एक कठोर सामाजिक ढांचा बन गया:
इतिहास में यह विभाजन उस समय शुरू हुआ जब 8वीं सदी में इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में आया। अरब, फारसी और मध्य एशियाई अभिजात वर्ग — जो अक्सर खुद को अशराफ (उच्च कुलीन) कहते थे — स्थानीय लोगों से मिले, जिनमें अधिकतर वे निम्नवर्गीय हिंदू थे जो ब्राह्मणवादी उत्पीड़न से मुक्ति चाहते थे। समय के साथ एक कठोर सामाजिक ढांचा बन गया:
अशराफ — (सैयद, शेख, पठान, मुगल): उच्च माने जाने वाले कुलीन वर्ग
अजलाफ़ — (कारीगर, किसान, जुलाहा): मध्यवर्गीय तबका
अरज़ल — (मजदूर, सफाईकर्मी, कसाई): सामाजिक रूप से बहिष्कृत वर्ग
अजलाफ़ और अरज़ल मिलकर पासमांदा कहलाते हैं, जो लगभग 85% भारतीय मुसलमानों का हिस्सा हैं। 1871 की ब्रिटिश जनगणना में उच्च जाति के मुसलमान मात्र 19% पाए गए थे।
आज भी अंसारी (जुलाहा), क़ुरैशी (कसाई), धोबी (धोबी) और फ़क़ीर जैसी समुदायों को शादी-ब्याह, मस्जिदों और मदरसों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी साक्षरता, आय और प्रतिनिधित्व आज भी अशराफ़ वर्ग से काफी कम है।
मौन बहुमत: पासमांदा प्रतिनिधित्व क्यों ज़रूरी है- संख्या में भारी होने के बावजूद, पासमांदा मुसलमानों को नेतृत्व के मंचों से लगभग बाहर रखा गया है, जहाँ अशराफ़ तबके का वर्चस्व कायम है। यह बहिष्कार केवल प्रतीकात्मक नहीं है — इसने आर्थिक ठहराव और सामाजिक अन्याय को स्थायी बना दिया है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ मुसलमानों की आबादी 3.8 करोड़ से अधिक है, पासमांदा वर्ग ग्रामीण और शहरी गरीबों की रीढ़ हैं। लेकिन राजनीति, शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।
ऑल इंडिया पासमांदा मुस्लिम महाज़ (AIPMM) इस परिवर्तन की अग्रणी शक्ति रही है। इसका नारा —
“दलित-पिछड़ा एक समान, हिन्दू हो या मुसलमान” ने देशभर में सामाजिक समानता और राजनीतिक भागीदारी की माँग को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। यह सत्य स्पष्ट करता है कि — सच्चा सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व से ही आरंभ होता है।
संवैधानिक आधार: न्याय के लिए कानूनी ढाँचा भारतीय संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ठोस ढाँचा तैयार किया है। अनुच्छेद 340, 341, और 342 राज्य को इन वर्गों की पहचान और सहायता का अधिकार देते हैं। मंडल आयोग (1979) इस दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इसकी 1980 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 52% आबादी पिछड़े वर्गों (OBC) में आती है, जिसमें लगभग 90% भारतीय मुसलमान शामिल हैं।
1990 में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया — जो पासमांदा समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक जीवनरेखा साबित हुआ।
इसके बाद 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ी जातियों की सूची में 76 समुदायों को शामिल किया, जिनमें 38 मुस्लिम पासमांदा समूह — जैसे जुलाहा, धुनिया, और फ़क़ीर — थे। यह मान्यता सामाजिक न्याय के मार्ग पर एक संस्थागत कदम थी।
2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू हुआ, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर अशराफ़ मुसलमान भी शामिल हैं।
ये सभी पहलें संविधान की सामाजिक न्याय की भावना और इस्लाम की पीड़ित के साथ खड़े होने की शिक्षाओं दोनों का प्रतीक हैं — जैसा कि पैग़म्बर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कहा:
“अपने भाई की मदद करो — चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम।”
इनकार की कीमत: सशक्तिकरण का छूटा अवसर
आज़ादी के बाद मुस्लिम नेतृत्व ने समुदाय के भीतर की जातिगत सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार किया। इस ‘एकरूप मुस्लिम पहचान’ के भ्रम ने आंतरिक असमानताओं को ढक दिया और पासमांदा व दलित मुसलमानों को आरक्षण और अवसरों से वंचित कर दिया।
आज मुसलमानों की संसद में भागीदारी 4–5% से अधिक नहीं है, जबकि उनकी आबादी 14% है — और इसमें पासमांदा का हिस्सा नगण्य है।
परिणामस्वरूप, अधिकतर पासमांदा आज भी पारंपरिक पेशों में सीमित हैं, जहाँ साक्षरता दर मात्र 50% है, जबकि अशराफ़ मुसलमानों में यह 70% से अधिक (जनगणना 2011) है। नेतृत्व में उनकी अनुपस्थिति गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक अदृश्यता के दुष्चक्र को बनाए रखती है।
नया सवेरा: राष्ट्रीय विमर्श में पासमांदा
आज़ादी के बाद पहली बार, पासमांदा प्रश्न भारत की राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विषय को नई पहचान और स्वीकार्यता मिली है। वर्ष 2017 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से “पासमांदा” शब्द का प्रयोग किया — जो भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक क्षण था।
इसके बाद, भोपाल (2023) से लेकर लखनऊ और पटना (2024) तक अपने भाषणों में उन्होंने बार-बार कहा कि —
“पासमांदा मुसलमानों की भागीदारी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।”
सरकार की छात्रवृत्तियाँ, मुद्रा योजना जैसी उद्यमिता योजनाएँ और मदरसा आधुनिकीकरण जैसी पहलें विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम वर्गों को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं।
AIPMM ने इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसने प्रधानमंत्री कार्यालय को कई नीति-आधारित रिपोर्टें सौंपी हैं, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं:
राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक सुधार. राष्ट्रीय विकास
इस सतत प्रयास का परिणाम है कि आज पासमांदा नेतृत्व नीति-निर्माण, सरकारी समितियों और मीडिया विमर्श में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
खाई को पाटना: समावेशी राजनीतिक नेतृत्व की दिशा में हाल के महीनों में कुछ मुस्लिम विचारकों ने समुदाय के भीतर सत्ता में भागीदारी के प्रश्न को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने यह भी पूछा है — क्या कुछ ही परिवार या अशराफ़ वर्ग ही हमेशा नेतृत्व पर क़ाबिज़ रहेंगे? और क्या उनके नेतृत्व में समुदाय की वास्तविक प्रगति हुई है?
वास्तविक परिवर्तन के लिए कुछ आवश्यक कदम हैं:
राजनीतिक सहमति बनाना: सभी मुस्लिम संगठनों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हाशिए पर पड़े वर्गों के विकास के लिए राजनीतिक संस्थानों में समान भागीदारी अनिवार्य है।
राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना: शिक्षित और संसाधन-संपन्न पासमांदा कार्यकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़कर अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से कार्य करना चाहिए।
नेतृत्व की जवाबदेही: राजनीतिक नेताओं को अपने समुदायों में शक्ति और अवसर के न्यायपूर्ण वितरण के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
मतदाताओं की भूमिका: मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो खुले तौर पर पिछड़े और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन करते हों।
धर्मनिरपेक्ष सहयोग: एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में अल्पसंख्यक तभी प्रभाव डाल सकते हैं जब वे अपने मतदान बल और संगठनात्मक एकता का विवेकपूर्ण उपयोग करें। भारत की 15% मुस्लिम आबादी, विशेषकर पासमांदा वर्ग, यदि एकजुट होकर संविधानिक ढाँचे में कार्य करें, तो वे नीति-निर्माण की दिशा बदल सकते हैं।
भविष्य की दृष्टि: इनकार से इज़्ज़त तक
पासमांदा संघर्ष केवल न्याय की माँग नहीं, बल्कि इज़्ज़त की पुनर्प्राप्ति की लड़ाई है — एक ऐसा आंदोलन जो सदियों की असमानता को समाप्त कर इस्लाम और संविधान के मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहता है।
मुस्लिम नेतृत्व को अब संकीर्ण पहचान राजनीति से ऊपर उठकर समानता, प्रतिनिधित्व और साझा प्रगति के मूल्यों को अपनाना होगा। कुरआन और संविधान दोनों इस सच्चाई पर एकमत हैं — मानव की कीमत उसके वंश में नहीं, बल्कि उसके कर्म और धर्मनिष्ठा में है।
AIPMM का नारा इस दृष्टि को साकार करता है — “पासमांदा मुस्लिम — सबका साथ, सबका विकास।” परिवर्तन का समय आने वाला नहीं है — वह समय अब है। आइए इस पीढ़ी को इतिहास बदलने दें — ताकि हर मुसलमान, चाहे वह पासमांदा हो या अशराफ़, गरिमा, समानता और अवसर के साथ जीवन जी सके।
 शारिक अदीब अंसारी
शारिक अदीब अंसारी
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऑल इंडिया पासमांदा मुस्लिम महाज़