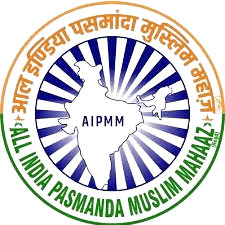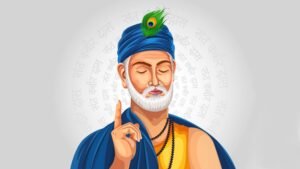 कबीर: जीवन, शिक्षाएं और योगदान- हज़रत संत कबीर रहमतुल्लाह अलैहे (लगभग 1398-1518) भारतीय उपमहाद्वीप के उन विरले महापुरुषों में से थे, जिन्होंने समाज के दोनों प्रमुख धर्मों—हिंदू और इस्लाम—की संकीर्णता, कर्मकांड और पाखंड को निर्भीकता से चुनौती दी। वे एक जुलाहा (अंसारी) समुदाय से थे, जो आज की सामाजिक शब्दावली में पसमांदा मुस्लिम समाज का हिस्सा है।
कबीर: जीवन, शिक्षाएं और योगदान- हज़रत संत कबीर रहमतुल्लाह अलैहे (लगभग 1398-1518) भारतीय उपमहाद्वीप के उन विरले महापुरुषों में से थे, जिन्होंने समाज के दोनों प्रमुख धर्मों—हिंदू और इस्लाम—की संकीर्णता, कर्मकांड और पाखंड को निर्भीकता से चुनौती दी। वे एक जुलाहा (अंसारी) समुदाय से थे, जो आज की सामाजिक शब्दावली में पसमांदा मुस्लिम समाज का हिस्सा है।
कबीर की वाणी निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, जो ईश्वर की एक निराकार, सर्वव्यापक छवि प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा:
“कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूँढै बन माहि।
कस्तूरी जैसी आध्यात्मिकता हमारे भीतर है, पर हम उसे बाहर खोजते रहते हैं।” उनकी रचनाएं जातिवाद, अंधविश्वास, धार्मिक वर्चस्व, और पाखंड पर सीधा प्रहार करती हैं। कबीर न तो हिन्दू बने और न ही मुसलमान, वे एक सार्वभौमिक मानवतावादी संत के रूप में उभरे।
संत कबीर की मृत्यु और दोनों धर्मों की प्रतिक्रिया- कबीर की मृत्यु के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके शरीर पर अंतिम संस्कार का अधिकार चाहते थे। किंवदंती है कि जब चादर हटाई गई, तो वहाँ केवल फूल मिले। दोनों समुदायों ने उन्हें बाँट लिया और अपने-अपने रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया।
यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे—वे पूरे मानव समाज के थे।
यदि संत कबीर किसी ‘सैय्यद’, ‘शेख’, ‘पठान’, ‘मिर्ज़ा’, या ‘मुगल’ वंश से होते, तो शायद उन्हें ‘वली’ घोषित कर दिया गया होता। पर क्योंकि वे पसमांदा समुदाय से थे, उनकी शिक्षाओं को दबाने का प्रयास हुआ।
कबीर की जयंती और उर्स: एक अदृश्य उत्सव- संत कबीर की जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है, और यह उर्स का रूप भी ले लेती है—खासकर पसमांदा मुस्लिम और कबीरपंथी समाजों में। 2025 में यह दिन 11 जून को पड़ा, लेकिन उर्दू मीडिया में इसकी उपेक्षा रही।
अशरफ मुस्लिम समाज (सैय्यद, शेख, मुगल, पठान आदि) में इस दिन पर कोई आधिकारिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी।
पसमांदा बनाम अशरफ: सामाजिक संरचना और भेदभाव- जातिगत असमानता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य- भारतीय मुस्लिम समाज में सदियों से अशरफ (उच्चवर्गीय) और अज्लाफ/अरज़ल (पसमांदा) के बीच सामाजिक भेदभाव चला आ रहा है। अशरफ अपनी जड़ों को अरब, ईरान या मध्य एशिया से जोड़ते हैं, जबकि पसमांदा समाज भारत के मूलनिवासी समाजों से आता है।
कबीर एक जुलाहा थे, और यही कारण था कि उन्हें न केवल ब्राह्मणों ने, बल्कि मुसलमानों के अशरफ वर्ग ने भी हाशिए पर रखा।
“धर्म के नाम पर जो सत्ता-लोलुपता है, उसने पसमांदा संतों को हमेशा दबाने का प्रयास किया है।”
2. धार्मिक संरचनाओं से दूरी- कबीर न तो चिश्ती, न कादरी, न शत्तारी, और न ही किसी सूफी सिलसिले के अनुयायी थे। उनकी निर्गुण भक्ति औपचारिक मज़हबी ढाँचों के बाहर थी। यही कारण है कि उनके विचार अशरफ धार्मिक नेतृत्व के लिए असहज थे।
3. मीडिया की मौन भूमिका- उर्दू मीडिया, जिस पर अधिकांशतः अशरफ वर्ग का प्रभुत्व है, ने न तो कबीर और न ही डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे पसमांदा मुस्लिम नायकों को बराबर का स्थान दिया।
हिंदी और अंग्रेजी मीडिया में कबीर की जयंती की कुछ कवरेज अवश्य हुई, परंतु वह भी सीमित दायरे में। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और कबीर: उपेक्षा का समान पैटर्न
डॉ. कलाम, जो मराइकार समुदाय (तमिलनाडु का पसमांदा मुस्लिम समाज) से आते थे, भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रनिर्माताओं में से एक रहे। लेकिन उर्दू मीडिया और कट्टर इस्लामी मंचों पर उनकी जयंती, उपलब्धियों, या मानवतावादी विचारों को नजरअंदाज किया गया। क्योंकि उनकी पहचान राष्ट्रवादी, वैज्ञानिक, और धर्मनिरपेक्ष थी, उन्होंने भी धार्मिक वर्चस्व की राजनीति से दूरी बनाई—और इसी वजह से उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया गया।
कबीर बनाम सूफी मजारें: एक विषमता
नीचे कुछ प्रमुख सूफी मजारें हैं जिन्हें अशरफ समुदाय में अत्यधिक महत्व दिया जाता है:
मजार संत सिलसिला सामाजिक वर्ग
अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सैय्यद
निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामुद्दीन चिश्ती सैय्यद
हाजी अली हाजी अली बुखारी बुखारी व्यापारी/शेख
देवा शरीफ वारिस अली शाह चिश्ती सैय्यद
गाज़ी मियां सालार मसूद योद्धा-संत सैय्यद
इन मजारों का व्यापक प्रचार, चढ़ावा, और उर्सों की परंपरा मजार-आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, जिसका सामाजिक लाभ अक्सर पसमांदा समुदाय तक नहीं पहुंचता।
लेकिन मगहर में कबीर की समाधि?
बिना प्रचार बिना सरकारी संरक्षण बिना धार्मिक संस्थानों की मदद के कबीर: एक पसमांदा संत और भारतीय मूल के नबी की परंपरा
जिस प्रकार नबी करीम ﷺ को मक्का के कुरैश ने सताया और अंततः उन्हें मदीना हिजरत करनी पड़ी, वैसे ही कबीर को भी सुल्तान सिकंदर लोदी के दौर में कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने भी सत्ता, वर्चस्व और जातीय धर्मशास्त्र से सीधी टक्कर ली—बिना डर, बिना लालच के। निष्कर्ष: कबीर और कलाम की उपेक्षा—सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, भविष्य का है क्या कारण है कि सच्चे संतों को, जो जातिवाद और धर्मान्धता के विरुद्ध खड़े हुए, आज भी नज़रअंदाज किया जाता है?
क्या यह केवल सामाजिक भूल है या सुनियोजित सांस्कृतिक बहिष्कार? अब समय है कि पसमांदा समाज अपने नायकों की पुनः प्रतिष्ठाहै करे, उन्हें मुख्यधारा विमर्श में स्थापित करे, और ‘धार्मिक वर्चस्ववाद’ के विरुद्ध आत्म-सम्मान की लड़ाई को तेज करे।