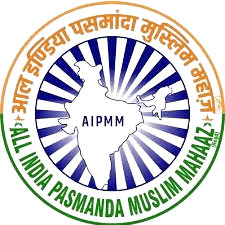भारत की सियासी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अब अपना ध्यान पसमान्दा मुसलमानों की ओर केंद्रित किया है — यानी वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान, जो भारत की मुस्लिम आबादी का लगभग 85% हिस्सा हैं (2005 के राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार)। वर्षों से मुख्यधारा की राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं से दूर रहे इन वर्गों की ओर भाजपा की बढ़ती दिलचस्पी महज चुनावी गणित नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम वोट बैंक की एकता को तोड़ने और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम पहचान की पारंपरिक समझ को पुनर्परिभाषित करने की एक साहसिक कोशिश है।
इस पूरी रणनीति का आधार है जातीय पहचान को धार्मिक एकता के ऊपर प्राथमिकता देना। आगामी 2026–27 की जनगणना के दौरान भाजपा पसमान्दा मुसलमानों को अपनी जातीय पहचान दर्ज कराने के लिए प्रेरित कर रही है—खासकर उस समय जब देश भर में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। इसका उद्देश्य है मुस्लिम उप-जातियों को ओबीसी आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाना। यह भाजपा की “सम्मान” और “संतुलन” की राजनीति का हिस्सा है, जो वह विपक्ष की “तुष्टीकरण” की राजनीति के बरक्स पेश करती है।
 पसमान्दा पहचान: मुस्लिम एकरूपता से परे- “पसमान्दा” शब्द पहली बार 1978 में डॉ. कामिल क़ैसरी और अब्दुल मजीद अदीब अंसारी द्वारा स्थापित “ऑल इंडिया तबकाती पसमान्दा फेडरेशन” के साथ सामने आया। यह शब्द मुस्लिम समाज के गैर-उच्चवर्गीय तबकों—अजलाफ़ (पिछड़े) और अर्ज़ल (दलित)—के लिए प्रयुक्त होता है, जो अशराफ़ (उच्च जातीय मुसलमानों) जैसे सैयद, शेख, मुग़ल और पठानों से अलग हैं। उत्तर प्रदेश में अंसारी (बुनकर), कुरैशी (कसाई), नाई (हज्जाम) जैसे समुदायों को ओबीसी में शामिल किया गया है, जबकि मंसूरी (धुनिया), इद्रीसी (दर्जी), और सैफी (लोहार) जैसे छोटे कारीगर तबके अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं—ओबीसी वर्ग में होने के बावजूद भी।
पसमान्दा पहचान: मुस्लिम एकरूपता से परे- “पसमान्दा” शब्द पहली बार 1978 में डॉ. कामिल क़ैसरी और अब्दुल मजीद अदीब अंसारी द्वारा स्थापित “ऑल इंडिया तबकाती पसमान्दा फेडरेशन” के साथ सामने आया। यह शब्द मुस्लिम समाज के गैर-उच्चवर्गीय तबकों—अजलाफ़ (पिछड़े) और अर्ज़ल (दलित)—के लिए प्रयुक्त होता है, जो अशराफ़ (उच्च जातीय मुसलमानों) जैसे सैयद, शेख, मुग़ल और पठानों से अलग हैं। उत्तर प्रदेश में अंसारी (बुनकर), कुरैशी (कसाई), नाई (हज्जाम) जैसे समुदायों को ओबीसी में शामिल किया गया है, जबकि मंसूरी (धुनिया), इद्रीसी (दर्जी), और सैफी (लोहार) जैसे छोटे कारीगर तबके अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं—ओबीसी वर्ग में होने के बावजूद भी।
जहां अशराफ नेतृत्व वाली मुस्लिम संस्थाएं धार्मिक पहचान को आगे रखती हैं, वहीं पसमान्दा आंदोलन सामाजिक न्याय और जातीय बराबरी पर ज़ोर देता है। यही वजह है कि भाजपा की यह पहल कुछ पसमान्दा नेताओं को स्वीकार्य लगती है, हालांकि संदेह बना हुआ है। भाजपा इसे ‘माइनॉरिटी आउटरीच’ नहीं, बल्कि जाति आधारित सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है—जो भारत की गहराई तक जाति से जुड़ी राजनीतिक संस्कृति में एक स्वाभाविक रणनीति है।
भाजपा की रणनीति: भाषण से प्रतिनिधित्व तक- 2022 में हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब “वंचितों और शोषितों” से जुड़ने की बात कही और खासतौर पर पसमान्दा मुसलमानों का उल्लेख किया, तभी से यह रणनीति सक्रिय हुई।
2023 के उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने 395 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे—जिनमें 90% पसमान्दा थे। इनमें से 61 प्रत्याशियों को जीत भी मिली।
भाजपा ने प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया है। 2022 में बलिया के पसमान्दा नेता दानिश आज़ाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और प्रमुख पसमान्दा आवाज़ प्रो. तारिक मंसूर को विधान परिषद का सदस्य और भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा अशराफ वर्चस्व वाली मुस्लिम राजनीति को चुनौती देने और अपनी ‘मुस्लिम विरोधी’ छवि को नरम करने की कोशिश कर रही है।
2023 के सुआर उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) ने शफीक़ अहमद अंसारी को मैदान में उतारा, जिन्होंने सपा प्रत्याशी को हराया। इसमें अलवी (फक़ीर), कुरैशी, सैफी, और अंसारी जैसे उप-जातियों की निर्णायक भूमिका रही—यह ज़मीनी स्तर पर पसमान्दा समर्थन में बदलाव का संकेत है।
जातिगत जनगणना: सबसे बड़ा दांव- भाजपा की रणनीति का सबसे अहम पहलू जातिगत जनगणना की वकालत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता कुँवर बसीत अली जैसे लोग खुलेआम मुसलमानों से जाति के आधार पर जनगणना में अपनी पहचान दर्ज कराने की अपील कर रहे हैं। इसके ज़रिए एक ऐसा ठोस डाटा तैयार किया जा सकता है, जो मुस्लिम समाज के भीतर आरक्षण के व्यापक विस्तार की मांग को मज़बूत आधार दे सके। इसे “अशराफ प्रभुत्व के ख़िलाफ़ सामाजिक न्याय की लड़ाई” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—वही सामाजिक न्याय जो कभी मंडल युग में सपा और राजद जैसी पार्टियों का प्रमुख हथियार था। लेकिन इस रणनीति में भी कई अंतर्विरोध हैं।
आलोचनाएं, विडंबनाएं और पसमान्दा समाज की सतर्कता- सिर्फ प्रतीकात्मकता काफी नहीं है—ऐसा कई पसमान्दा लोग मानते हैं। मुरादाबाद के पीतल कारीगर दिलशाद हुसैन ने 2022 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात की थी। उन्होंने सम्मान के लिए सराहना की, पर कहा कि “ज़मीनी विकास अब भी नदारद है।” वहीं मलिक जाति से ताल्लुक रखने वाले सब्ज़ी विक्रेता साहिब-ए-आलम मानते हैं कि जातिगत पहचान ज़रूरी है, लेकिन भाजपा की मंशा को वे चुनावी नज़र से ही देखते हैं।
इस रणनीति से मुस्लिम समाज के भीतर तनाव भी पैदा हुआ है। पसमान्दा नेताओं पर सोशल मीडिया पर अशराफ तबकों द्वारा जातिगत गालियाँ जैसे “जुलाहा” जैसी टिप्पणियाँ की गईं। भाजपा इसके जवाब में यह तर्क देती है कि अब तक अशराफ नेतृत्व ने ही सरकारी लाभों का एकाधिकार बना रखा था—इसलिए अब ज़रूरत है मुस्लिमों के भीतर संसाधनों के न्यायपूर्ण पुनर्वितरण की।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है—भाजपा की व्यापक हिंदुत्व नीति। “सम्मान” और “समावेशन” की बातों के बीच बहुत से पसमान्दा आज भी उस भाजपा से सतर्क हैं, जिसकी छवि मुस्लिम विरोध, बुलडोज़र राजनीति, मदरसों के प्रति संदेह, और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी है। जब तक ठोस नीतिगत बदलाव नहीं होंगे—जैसे कि दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करना, या निजी क्षेत्र में ओबीसी कोटा लागू करना—तब तक सिर्फ प्रतीकात्मक नियुक्तियाँ विश्वास नहीं जीत सकेंगी।
वोटों का असर भी सीमित रहा है। 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनावों में भाजपा के चार पसमान्दा मुस्लिम प्रत्याशियों में से कोई नहीं जीत सका—हालाँकि एक प्रत्याशी बहुत क़रीब पहुँचा। पार्टी के पास अब भी कोई मुस्लिम सांसद नहीं है और वह मुस्लिम मतदाताओं के बीच अब भी सीमांत भूमिका में है।
आगे क्या? पंचायत से विधानसभा तक- आगामी वर्षों में भाजपा की यह रणनीति कितनी स्थायी है, यह 2026 के पंचायत चुनावों से लेकर 2027 के विधानसभा चुनावों तक में स्पष्ट होगा। खासकर आज़मगढ़, रामपुर, मुरादाबाद जैसे ज़िलों में भाजपा का ज़मीनी नेटवर्क और पसमान्दा जागरूकता परीक्षा में खड़ा होगा।
भाजपा अब कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना को “पसमान्दा गौरव” के आख्यान से जोड़ने की कोशिश कर रही है—जिसमें वीर अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र विजेताओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पर असली चुनौती तब पार होगी, जब ये प्रतीकात्मकता हकीकत में उन नीतियों में बदलेगी जो पसमान्दा समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में ठोस सुधार लाए।
कांग्रेस अपने 2012 के ‘अल्पसंख्यक उप-कोटा’ प्रस्ताव को फिर से ज़िंदा कर सकती है। सपा धार्मिक एकता के पुराने तर्क को मज़बूत कर मुस्लिम समर्थन बनाए रखने की कोशिश करेगी। इन विभिन्न रणनीतियों का परिणाम ही यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश और शायद भारत का अगला राजनीतिक नक्शा कैसा होगा।
मुस्लिम राजनीति का पुनर्लेखन? भाजपा की पसमान्दा तक पहुंच महज़ एक राजनीतिक दांव नहीं है, यह भारतीय राजनीति में चल रहे गहरे बदलाव की ओर इशारा करती है—जहां धार्मिक एकता की जगह अब जातीय अस्मिता को प्राथमिकता मिल रही है, और धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की पुरानी बहस अब जटिल सामाजिक गणित में बदल रही है।
पसमान्दा समुदाय के सामने यह एक निर्णायक मोड़ है—वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को दोबारा परिभाषित कर सकते हैं। यह ‘सशक्तिकरण’ बनता है या ‘सत्ता में समावेशन के नाम पर को-ऑप्टेशन’—यह सिर्फ भाजपा के वादों पर नहीं, बल्कि विपक्षी दलों, नागरिक समाज, और खुद पसमान्दा समाज की सूझबूझ पर भी निर्भर करेगा। जैसे-जैसे जनगणना और आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भारत की राजनीतिक ज़मीन फिर से खींची जा रही है। इस नए नक्शे के केंद्र में हैं पसमान्दा—वो समुदाय जिसे दशकों तक हाशिए पर रखा गया, और जिसे अब हर ओर से पुकारा जा रहा है।

शारिक अदीब अंसारी
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
ऑल इंडिया पसमान्दा मुस्लिम महाज़