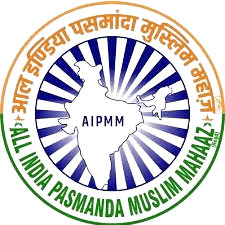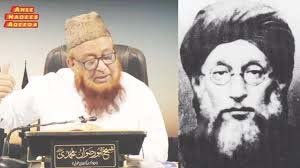 उर्स और पहचान- मौलाना अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी का उर्स हर साल बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बरेली शरीफ़ (उत्तर प्रदेश) में उनके मज़ार पर लाखों की भीड़ जमा होती है। यह वही अहमद रज़ा ख़ान हैं जिन्हें “आला हज़रत” कहा जाता है और जिन्होंने बरेलवी मसलक की बुनियाद रखी थी।
उर्स और पहचान- मौलाना अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी का उर्स हर साल बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बरेली शरीफ़ (उत्तर प्रदेश) में उनके मज़ार पर लाखों की भीड़ जमा होती है। यह वही अहमद रज़ा ख़ान हैं जिन्हें “आला हज़रत” कहा जाता है और जिन्होंने बरेलवी मसलक की बुनियाद रखी थी।
अहमद रज़ा ख़ान का संक्षिप्त जीवन-परिचय
पूरा नाम: अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी
जन्म: 14 जून 1856 ई. (10 शव्वाल 1272 हिजरी), बरेली (उत्तर प्रदेश, भारत)
इंतिक़ाल: 28 अक्टूबर 1921 ई. (25 सफ़र 1340 हिजरी)
कम उम्र से ही उन्होंने दीन की तालीम हासिल की और फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर वगैरह में महारत पाई।
बरेलवी मसलक की बुनियाद
अहमद रज़ा ख़ान ने कोई नया मज़हब नहीं बनाया, बल्कि हनफ़ी मसलक के भीतर रहते हुए एक “बरेलवी तहरीक” की शुरुआत की। यह तहरीक लगभग 1880–1900 ई. के बीच आकार लेती है। उनका दावा था कि वे अहले-सुन्नत वल-जमाअत की असली नुमाइंदगी कर रहे हैं। विरोधियों (देवबंदी, अहले-हदीस आदि) ने उन्हें और उनके अनुयायियों को “बरेलवी” कहना शुरू किया, और यही नाम मशहूर हो गया।
ख़ास बातें- बरेलवी तहरीक का केंद्र बरेली शहर रहा। अहमद रज़ा ख़ान ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा नहीं दिया, बल्कि उन्हें “जिम्मी हुकूमत” मानकर तआवुन (सहयोग) का रवैया अपनाया। उन्होंने अपनी मशहूर किताब फ़तवा-ए-रिज़विया (30 जिल्दों में) में पसमांदा समाज, देवबंदी उलमा और दूसरे मसलकों के ख़िलाफ़ बेहद सख़्त और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- उन्नीसवीं सदी के आख़िरी दौर में भारतीय मुसलमानों का धार्मिक नेतृत्व ज़्यादातर सैयदों और अशराफ वर्ग (सैयद, शेख़, पठान, मुग़ल) के हाथों में था। ऐसे हालात में अहमद रज़ा ख़ान ने बरेलवी तहरीक की बुनियाद रखी।
कहा जाता है कि यह तहरीक महज़ धार्मिक सुधार का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे पठानों के सामाजिक-धार्मिक वर्चस्व को बनाए रखने की राजनीति भी थी।
बरेलवी मसलक और पसमांदा समाज- विडंबना यह है कि आज इस मसलक के सबसे बड़े अनुयायी पसमांदा मुसलमान हैं—जैसे कसाई, नाई, बुनकर, दर्जी, धोबी, तेली, मल्लाह, लोहार, कहार और अन्य जातियाँ। लेकिन हक़ीक़त यह है कि अहमद रज़ा ख़ान ने अपनी किताब फ़तवा-ए-रिज़विया में बार-बार इन्हीं जातियों को “नीचा”, “रज़ील” और “घटिया” कहकर सामाजिक रूप से अपमानित किया।
फ़तवा-ए-रिज़विया से मिसालें
1. पसमांदा जातियों को नीचा बताना
अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा कि अशराफ मुसलमानों के लिए पसमांदा जातियों (जैसे कसाई, नाई, धोबी, तेली) से रिश्ता जोड़ना (शादी-ब्याह करना) नाजायज़ और ज़लील करने वाला काम है।
> “शरीफ़ अपनी औलाद को नीच जातियों में देकर ज़लील न करें।”
(फ़तवा-ए-रिज़विया, जिल्द 7, सफ़ा 441–445)
2. ‘रज़ील’ और ‘नीच’ कहना
एक जगह उन्होंने लिखा:
> “कसाई, जुलाहा (बुनकर), नाई, धोबी, तेली, चमार आदि ज़ातों में शरीफ़ अपनी बेटियों का निकाह करना ज़िल्लत है।”
(फ़तवा-ए-रिज़विया, जिल्द 6, सफ़ा 159)
L
3. सोशल बहिष्कार का फ़तवा- बार-बार चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अशराफ मुसलमानों को पसमांदा जातियों से “बराबरी का रिश्ता” नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह शरीअत के ख़िलाफ़ है।
विडंबना और मानसिक गुलामी- इन मिसालों से साफ़ है कि अहमद रज़ा ख़ान ने पसमांदा मुसलमानों को कभी बराबरी का हक़दार नहीं माना। उन्होंने उन्हें “नीच”, “रज़ील” और “ज़िल्लत” का पात्र बताया। इसके बावजूद, आज यही पसमांदा समाज उनके उर्स में सबसे बड़ी तादाद में शामिल होता है, चादर चढ़ाता है और उन्हें धार्मिक “आदर्श” व “मसीहा” मानता है। यह स्थिति पसमांदा समाज की गहरी मानसिक गुलामी और सामाजिक शोषण को उजागर करती है—जहाँ अपमान करने वाला ही पूजनीय बना बैठा है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को “अफ़ीम” कहा था। बरेलवी मसलक के अनुयायियों को देखकर यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। लोग दूर-दराज़ से, भयंकर गर्मी और तंगी के बावजूद, उर्स में शामिल होने आते हैं। उनके घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता, बच्चों के लिए दवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं होता, फिर भी वे उधार लेकर उर्स में शामिल होने पहुँचते हैं। और विडंबना यह है कि इनमें 90% वही पसमांदा मुसलमान हैं, जिन्हें अहमद रज़ा ख़ान ने अपनी किताब में “रज़ील” और “कमें” कहा था।
👉 अब सवाल यह है कि जो नेता और मौलाना आपकी सामाजिक बराबरी तक नहीं मानते, क्या उन्हें अपना “मसीहा” मानना किसी भी तरह से समझदारी है?