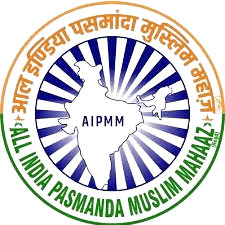राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अक्टूबर 2025 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह क्षण केवल किसी संगठन की औपचारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी स्थायी एकता, अनुशासन और संगठनात्मक शक्ति का सजीव प्रमाण है। एक ऐसे युग में, जहाँ बिखराव, गुटबाज़ी और विघटन आम हो गए हैं, आरएसएस का सौ वर्षों तक निरंतर सक्रिय और प्रभावशाली बने रहना निस्संदेह असाधारण है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अक्टूबर 2025 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह क्षण केवल किसी संगठन की औपचारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी स्थायी एकता, अनुशासन और संगठनात्मक शक्ति का सजीव प्रमाण है। एक ऐसे युग में, जहाँ बिखराव, गुटबाज़ी और विघटन आम हो गए हैं, आरएसएस का सौ वर्षों तक निरंतर सक्रिय और प्रभावशाली बने रहना निस्संदेह असाधारण है।
1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क्स में से एक है। लाखों स्वयंसेवक सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकता के कार्यों में समर्पित हैं। किसी के लिए यह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है, तो किसी के लिए राजनीतिक प्रभाव का स्रोत। किंतु निर्विवाद तथ्य यह है कि संघ ने अपने सौ वर्षों में न केवल टिकाऊपन साबित किया है, बल्कि विस्तार और संगठित शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।
एक पसमांदा मुसलमान और वंचित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, मैं संघ को न तो पक्षपात से देखता हूँ और न ही शत्रुता की दृष्टि से, बल्कि एक अध्ययन के रूप में कि कैसे संगठनात्मक एकता पीढ़ियों तक जीवित रह सकती है। यह प्रश्न हर सामाजिक आंदोलन के लिए महत्त्वपूर्ण है: प्रतिबंधों, संकटों और वैचारिक चुनौतियों के बीच कोई संगठन कैसे बिखरता नहीं और कैसे टिकाऊ बनता है?
ऐतिहासिक नींव और नेतृत्व का संक्रमण- आरएसएस का उदय औपनिवेशिक अशांति के दौर में हुआ, जब भारत की सबसे बड़ी कमजोरी असंगठन और गुटबाज़ी मानी जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन की गुटीय राजनीति से निराश होकर डॉ. हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया, जिसका केंद्रबिंदु आंदोलनकारी राजनीति नहीं, बल्कि अनुशासन और चरित्र निर्माण हो। शाखा पद्धति के माध्यम से यह दृष्टि जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले सकी।
1940 में नेतृत्व माधव सदाशिव गोलवलकर “गुरुजी” को मिला, जिन्होंने संघ की स्थायी दिशा निर्धारित की। यह संक्रमण इस बात का संकेत था कि संघ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक विचारधारा और संगठन की अखंडता को प्राथमिकता देता है।
राजनीति से दूरी और प्रभाव- स्वतंत्रता के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीतिक मंच खड़ा करने के लिए सहयोग माँगा, तब भी संघ ने स्पष्ट किया कि वह किसी दल की “पूंछ” नहीं बनेगा। फिर भी व्यावहारिकता अपनाते हुए दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख जैसे प्रचारकों को 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में सहयोग की अनुमति दी गई। इस संतुलन ने संघ को संगठनात्मक स्वतंत्रता भी दी और राजनीति में अप्रत्यक्ष प्रभाव की क्षमता भी।
एकता के तीन स्तंभ
संघ की दीर्घकालिक एकता तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी है—
1. विचारधारा: हिंदुत्व का दर्शन स्वयंसेवकों को दीर्घकालिक दृष्टि और वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है।
2. संरचना: शाखा व्यवस्था बाल्यावस्था से ही अनुशासन, भाईचारा और सांस्कृतिक गर्व की शिक्षा देती है।
3. संकट प्रबंधन: प्रतिबंधों और कठिन परिस्थितियों—1948, 1975 और 1992—ने संगठन को और मज़बूत किया।
नेतृत्व परिवर्तन भी हमेशा सहज और अनुशासित रहा—हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक। शायद ही कोई अन्य भारतीय संस्था इतनी स्थिर उत्तराधिकार परंपरा का दावा कर सके।
आलोचनाएँ और योगदान
आलोचक अक्सर कहते हैं कि संघ स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका में नहीं रहा। यह सही है कि उसने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आयोजित नहीं किए, परंतु ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने संघ की गतिविधियों पर गहन निगरानी रखी और कई स्वयंसेवकों पर क्रांतिकारियों को सहयोग देने के आरोप लगे। संघ ने राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष राजनीति से अधिक अनुशासन और चरित्र निर्माण की भूमिका निभाई।
साथ ही, संघ ने सामाजिक सेवा के माध्यम से स्वयं को केवल “कैडर फैक्ट्री” तक सीमित नहीं रखा। सेवा भारती और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में उसकी गहरी पैठ बनी।
पसमांदा दृष्टिकोण और भविष्य की चुनौती
आज जब संघ शताब्दी मना रहा है, भारत के अन्य सामाजिक आंदोलनों के लिए उसका संदेश स्पष्ट है—अनुशासन और एकता से ही दीर्घकालिक शक्ति मिलती है। किंतु यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि यह शक्ति विभाजनकारी न होकर समावेशी हो। पसमांदा मुसलमानों और अन्य वंचित समूहों के लिए यही सबसे बड़ी सीख है।
संघ की यात्रा हमें यह बताती है कि अनुशासन और विचारधारा से टिकाऊ संगठन बनाए जा सकते हैं। किंतु भारत की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति तभी होगी जब संगठनात्मक शक्ति का संगम न्याय और समावेशिता से होगा।
मेरे राय में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी केवल उसकी उपलब्धियों का स्मरण नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का अवसर है कि संगठित शक्ति इतिहास में अपार महत्व रखती है। असली कसौटी यह होगी कि यह शक्ति भारत की विविधता और सबको साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण से कितनी जुड़ती है।
एक पसमांदा मुसलमान के रूप में, मैं संघ की यात्रा में प्रेरणा भी देखता हूँ और सावधानी का संदेश भी। प्रेरणा इस बात की कि अनुशासन और समर्पण से संगठन कैसे जीवित रहते हैं, और सावधानी इस बात की कि सच्ची शक्ति वही है जो सबको ऊपर उठाए। प्रश्न यह है—क्या आने वाला भारत ऐसा हो सकता है जहाँ यह एकता किसी एक पहचान के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों की साझा नियति के लिए हो? यदि हाँ, तो यही एकता न्याय और समानता की नींव बन सकेगी।
शारिक अदीब अंसारी
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़